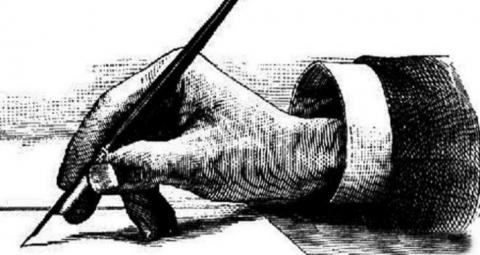अचानक पत्रकार बिरादरी के कुछ मित्रों को पत्रकारिता में ‘निष्पक्षता’ और ‘तटस्थता’ याद आने लगी है. कहा जा रहा है कि पत्रकार को ‘वाद’ से परे रहना चाहिए. कि पत्रकार को किसी पक्ष से निकटता या दूरी नहीं रखनी चाहिए. इसका मतलब यदि सिर्फ यह है कि रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है. पत्रकार को बेईमान तो नहीं ही होना चाहिए. हालांकि वित्तीय लोभ में या निजी निकटता/खुन्नस के कारण रिपोर्टिंग में भी डंडी मारने की बात छोड़ दें, तो दलीय/वैचारिक आग्रहों के कारण भी अपवादों को छोड़ अमूमन थोड़ी बहुत बेईमानी करते ही हैं. मगर पत्रकार बिरादरी तो हमेशा से दलीय और वैचारिक आधार पर खेमों में बंटी रही है. पहले की बात छोड़ भी दें, तो मैंने लगभग 22 वर्षों की पत्रकारिता में यही देखा है. कांग्रेसी, वामपंथी, भाजपाई या संघी हर किस्म के पत्रकार रहे हैं. कोई सत्ता पक्ष के निकट होता है, कोई विपक्ष के. इसमें कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है. लेकिन गड़बड़ तब होती है, जब वह खबर में मिलावट करने लगता है, तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने लगता है. और सबसे अधिक तब, जब उसके सार्वजनिक व्यवहार में यह पक्षधरता दिखने लगती है.
पत्रकार एक नागरिक भी होता है. उससे जागरूक, संवेदनशील होने और सामाजिक सरोकार रखने की अपेक्षा भी की जाती है. जाहिर है, वह विचार-शून्य नहीं हो सकता. समाज में चल रही धाराओं और विचारधाराओं से परे और निरपेक्ष भी नहीं. उसे भरसक निष्पक्ष होना चाहिए, पर तटस्थ होना कतई जरूरी नहीं. आज की तारीख में बेशक पत्रकारिता भी एक अदद नौकरी ही है. ऐसे में संभव है कि बहुतेरे पत्रकार जोखिम उठाने से डरते हों, बल्कि डरते ही हैं. लेकिन इस कारण सबों को बेईमान कहना/मान लेना भी जायज नीं लगता.
मुझे लगता है, यह सवाल गौरी लंकेश की हत्या के बाद और कारण ही उठे या उठाये जा रहे थे; और उसके बाद से सेकुलर और वामपंथी रुझान वाले पत्रकारों के सही-गलत पक्षपात के उदहारण दिये जाते रहे हैं. मकसद स्पष्ट है- जो पत्रकार मौजूदा सरकार और सत्तारूढ़ जमात की आलोचना करते हैं, वे कितने एकांगी और पक्षपाती हैं, यह साबित करना. मैं किसी रवीश कुमार, बरखा दत्त या राजदीप सरदेसाई आदि का बचाव नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ तसवीर का दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूं.
’74 आंदोलन के दौरान एक्सप्रेस ग्रुप के अखबार खुलेआम आंदोलन का पक्ष लेते थे. इंडियन एक्सप्रेस (बाद में ‘जनसत्ता’) तो मानो आंदोलन का मुखपत्र ही बन गया था. आज जो लोग पत्रकारों के किसी विचारधारा या वाद से जुड़ने या किसी दल के अंधविरोध की बात करते हैं, वे एक्सप्रेस और ‘जनसत्ता’ के उस अंदाज पर क्या कहेंगे?
जब वर्ष ’86 में मैं बतौर उप-संपादक एक अखबार (प्रभात खबर) से जुड़ा, तब उसके मालिक एक कांग्रेसी (अब दिवंगत) थे. स्वाभाविक ही अखबार की छवि कांग्रेसी अखबार की थी. हालाँकि सम्पादकीय मामलों में वे कोई हस्तक्षेप करते थे, मुझे इसका कभी एहसास नहीं हुआ. हां, एक अघोषित शर्त थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की छवि और कांग्रेस के सीधे खिलाफ कोई आक्रामक खबर-लेख न छपे. लेकिन संपादक थोड़ी ‘अतिरिक्त सावधानी’ बरतते थे. तब मैं घोर कांग्रेस विरोधी हुआ करता था. सप्ताह में एक दिन मुझे नेशनल पेज देखना होता था. अपने राजनीतिक रुझान के तहत मैं तत्कालीन विपक्षी दलों-नेताओं से जुडी ख़बरों को तरजीह देता. कुछ मित्र अचरज करते, कहते- ये क्या कर रहे हैं? मैं कहता- मुझे तो ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है. जो सही लगता है, लगाता हूं. पेज पर राष्ट्रीय महत्त्व का एक चित्र भी लगता था, जो उसी दिन के किसी राष्ट्रीय अखबार से लेकर लगाया जाता. वह फोटो भी मैं विपक्षी दल के किसी कार्यक्रम या नेता – वाजपेयी, जार्ज आदि- की लगा देता. सुबह अख़बार देख कर पता लगता कि कुछ ख़बरें और तस्वीरें बदल गयी हैं. पूछने पर बताया जाता कि संपादक के आदेश से हुआ. तो क्या मैं पक्षपाती था?
वह देश में उथल-पुथल का दौर था. पंजाब जल रहा था. अयोध्या में सुगबुगाहट शुरू हो गयी थी. ’89 तक आते-आते सारे देश में अयोध्या की आंच पहुँचने लगी थी. उसी आंच के क्रम में भागलपुर में भीषण दंगा भी हुआ. तब तक प्रभात खबर का स्वामित्व बदल गया. नये संपादक (हरिवंशजी) आ गये; और अचानक अखबार कांग्रेस विरोधी हो गया. हम जैसों को मजा आ गया. केंद्र में सरकार बदल गयी. ’90 में बिहार और यूपी में भी. उधर अयोध्या में गतिविधियाँ तेज हो रही थीं और सारा देश उसकी चपेट में आता जा रहा था. तभी प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी. अचानक वीपी खलनायक बन गये. लालू प्रसाद और मुलायम सिंह भी. देश की हिन्दी पट्टी मंडल-कमंडल खेमों में बंट गयी. अचानक कल तक मॉडरेट और प्रगतिशील छवि के बहुतेरे लोगों की ‘उदारता’ उजागर हो गयी. पत्रकार बिरादरी भी अछूती नहीं थी.
अब जरा पत्रकार बिरादरी के सामजिक चेहरे और बनावट पर गौर कर लें. हमारे अखबार के संपादकीय विभाग में तब एक भी आदिवासी, दलित या ईसाई नहीं था. दो-तीन मुसलिम और शायद इतने ही कथित पिछड़ी जातियों के. शेष कौन थे, बताने की जरूरत नहीं है. बेशक उनमें कुछ कांग्रेस और वाम धारा से जुडे थे. पर अधिकतर ‘कमंडल’ थाम चुके थे. दक्षिण भारत में कहीं आरक्षण के विरोध में कोई जुलूस निकला; और एक अखबार में शीर्षक लगा : दक्षिण में भी फैली आरक्षण विरोधी लहर! मेरा आकलन है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा देने में, उसे अतिरिक्त कवरेज देने में पत्र-पतिकाओं, यानी पत्रकारों (खास कर हिन्दी के) की भूमिका अत्यंत पक्षपातपूर्ण थी. नकारात्मक थी.
’90 में आडवाणी जी की रथ यात्रा झारखंड होकर गुजरी. सारे अखबार ‘राममय’ नजर आ रहे थे. प्रभात खबर बेशक संतुलित था (मूलतः सम्पादक के कारण), मगर जब रिपोर्टर और डेस्क एक रंग में रंग गया हो, तो वह संतुलन भी कितना रह सकता था. श्री आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया. रांची में कर्फ्यू लग गया. अफवाहों का दौर चल रहा था और इसमें कुछ अख़बारों की भी भूमिका थी.
’92 तक माहौल और विषाक्त हो चुका था. छह दिसंबर को सुबह से तनाव का माहौल था. आशंका थी कि आज कुछ गड़बड़ हो सकती है. मैं लोगों के मना करने के बावजूद दफ्तर पहुँच गया. तब तक टेलीप्रिंटर से ही तजा खबर मिलती थी. यूपी मूल के एक वरिष्ठ पत्रकार (जिनकी संघ से निकटता थी; और जो अब नहीं रहे) को अलग टेलीफोन उपलब्ध कराया गया था, ताकि वे अपने ‘खास स्रोत’ से ताजा जानकारी जुटा सकें. कुछ कुछ देर में वे सीधे लखनऊ और अयोध्या से मिली विस्फोटक जानकारी प्रसारित करते. उनमें से अधिकतर बाद में अफवाह ही साबित हुईं. एक एक कर मस्जिद के गुम्बद गिरने की सूचना मिलती रही. हम कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी, पर कुल मिला कर सम्पादकीय विभाग में चिंता जैसा कोई माहौल नहीं था!
अगले दिन के कुछ अखबारों में शीर्षक थे- ‘कारसेवकों के खून से सरयू का पानी लाल हो गया’.. ‘अयोध्या की सड़कें कारसेवकों की लाशों से पट गयीं’ आदि आदि. यह ‘निष्पक्ष पत्रकारिता थी.
उसके बाद हुए प्रत्येक चुनाव; यहाँ तक कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भी, सम्पादकीय कक्ष का माहौल कुछ अजीब हो जाता. मानो ‘कमल’ ही खिला होता था! ’96 का चुनावी नतीजा आ रहा था. तब तक टीवी आ चुका था. एक एक सीट का रिजल्ट (यदि भाजपा के पक्ष में हो) आने पर क्रिकेट में चौके-छक्के लगने पर होने जैसा शोर और जश्न का माहौल हैरान कर देता था. उसके बाद के प्रत्येक चुनाव में यही नजारा होता था. जब एक ’प्रतिष्ठित’ अखबार के सम्पादकीय कक्ष का माहौल ऐसा था, तो कल्पना की जा सकती है कि पत्रकारिता कितनी ‘तटस्थ’ होती होगी. आज की तो बात ही छोड़ दें.
यह गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है. वातावरण में उसी तनाव और गंध का एहसास तो होने ही लगा है; और अतीत के गड़े मुर्दों पर राजनीति तो हो ही रही है.
हम निष्पक्ष रह सकते हैं, रहना भी चाहिए. मर्यादित भी. मगर तटस्थ रहना कोई आदर्श नहीं है. पत्रकार के लिए भी नहीं. खास कर जब देश और समाज में उथल-पुथल की स्थिति हो, उदारता और संकीर्णता के बीच टकराव की स्थिति हो. न्याय और अन्याय के बीच आप तटस्थ कैसे रह सकते हैं. दिनकर के शब्दों में ‘...जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध..’